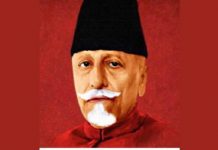मैं भारत में पैंतीस वर्षों से ज्यादा समय से पत्रकारिता और पत्रकारिता के अकादमिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहा हूं। मेरे पत्रकारिता के अनुभवों में आए शब्दों में सबसे पहले नंबर पर एक शब्द आता है वह है जाति। मैं ब्रिटेन के अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव और उनके आंदोलनों से वाकिफ हूं। दुनिया में लिंग, रंग, नस्ल, भाषा, धर्म आदि स्तरों पर भेदभाव होते रहे हैं। भेदभाव का मतलब यह देखने को मिलता है कि जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर ऊपर बैठा है, वह इन आधारों पर एक बड़ी आबादी को अपने अधीन रखना चाहता है। भारत में जब ब्रिटिश हुकूमत थी तब राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव होते थे। तब भारत में ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह गुहार लगायी जाती थी कि भारत के लोगों को भी नौकरियों में जगह दी जाए। उन्हें भी आत्म सुरक्षा का अधिकार दिया जाए। भारतीयों द्वारा ऐसी मांगों की एक लंबी फेहरिस्त हैं।
दुनिया भर के भेदभाव के जो कारण हैं, भारत में उनसे एक बिल्कुल भिन्न कारण है जिसे हम जाति के नाम से जानते हैं। देश के संविधान के अनुसार आप धर्म बदल सकते हैं। विज्ञान जेंडर में बदलाव की सहूलियत देता है। लेकिन भारत में जाति नहीं बदली जा सकती। हर चीज पर जाति का ठप्पा मिलता है। रंगों में जाति हैं। जाति के श्मशान है। जाति में ही शादियां होती हैं। नामों में जातीय विभाजन हैं।
मैं यदि एक सीधा सवाल करूं कि आखिर भारत के बीबीसी कार्यालय में देश की लगभग नब्बे प्रतिशत आबादी का कोई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? क्यों खास तरह के जातीय वर्ग के लोग बीबीसी में पसंद किए जाते रहे हैं। जो पसंद करने वाले रहे हैं, क्या वह एक खास तरह से सोचने, उठने-बैठने, हंसने, मिलने-जुलने, लिखने-पढ़ने, पहनावे आदि को पसंद करते रहे हैं? क्या यह जाति नहीं है? जिन्हें पसंद नहीं किया जाता रहा है, क्या उन्हें केवल इसीलिए खारिज किया गया कि उन्हें अच्छी भाषा में लिखने व पत्रकारिता की समझ नहीं है? आप जिसे योग्यता कहते हैं, वह दरअसल एक पैकेजिंग है और भारत में योग्यता की पैकेजिंग की कसौटी जाति होती है। हम लोगों ने 2006 में जब भारत के लगभग सभी मीडिया संस्थानों के सम्पादकीय विभागों में सबसे ऊपर के पदों पर बैठने वाले लोगों की जातीय पृष्ठभूमि के बारे में एक अध्ययन किया तो पाया कि नब्बे फीसदी आबादी के बीच के लोग इन दफ्तरों में बैठने के लिए जगह नहीं पाते हैं। इन संस्थानों में बीबीसी का भारत का कार्यालय शामिल भी था।
क्या यह सिर्फ संयोग है कि जिन्हें इन दफ्तरों में रखा गया, वे सभी योग्य लोग खास जाति वर्ग के लोग ही निकलते हैं। यानी नजर ऐसी है जो केवल खास जाति वर्ग को पसंद कर पाती है।
आप स्वयं सोचें कि जाति का ऐसा पैनापन और गहरा प्रभाव किस तरह से किसी सार्वजनिक जगह पर काम करता होगा। एक जाति को अपवित्र माना जाता है। एक जाति की परछाई नफरत के लिए होती है। क्या इस तरह छुआछूत और नफरत को मानने वालों के बीच से आने वाले लोगों के बारे में यह मान लिया जाए कि वे दफ्तर पहुंचकर बीबीसी जैसी संस्था के वैश्विक मुलाजिम के रूप में खुद को परिवर्तित कर लेते हैं? जिन्हें हजारों वर्षों का जाति भेद का प्रशिक्षण मिला हुआ है।
भारत में ब्रिटिश सत्ता के लौट जाने के बाद सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर सत्ता में भागीदारी की मांग राजनीति के केन्द्र में बनी रही है। ब्रिटिश-भारत में जो लोग भारतीय के नाम पर अपने लिए सरकारी सेवा में मौका देने की मांग करते रहे हैं, वहीं लोग 1947 के बाद भी भारत में व्यावहारिक स्तर पर हुकूमत कर रहे हैं और उन्होंने ही सदियों से सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ा रखने के कानून बनाए हैं और उनसे अब उन वैदिक कानूनों को व्यावहारिक स्तर पर खत्म करने की मांग की जाती है। लेकिन एक भेदभाव बराबरी के बीच दूरी को खत्म करने के लिए होता है और दूसरा भेदभाव वास्तव में नफरत होता है और वह खत्म करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे घृणास्पद बनाए रखा जाता है।
आखिर बीबीसी में भारतीय समाज के पिछड़े वर्ग, दलितों-आदिवासियों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिखाई देता है? दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी तीन हजार से ज्यादा जातियों के समूहों का सरकारी नाम है। क्या वे काले होते हैं? क्या उनके उठने-बैठने का तरीका अलग है। क्या उनके सोचने का तरीका वैसा है जैसा कि भारतीय संविधान का है? क्या उन्हें कब किसके सामने होंठों पर हल्की मुस्कुराहट देनी है ये नहीं आता। हंसते है तो तेज आवाज होती है और वर्चस्ववादी संस्कृति में उसे असभ्य माना जाता है? भारत में जाति की पहचान के लिए चूहे और चीटी की नाक लगी होती है।
मैं आपको ये लंबा खत क्यों लिख रहा हूं क्योंकि आपके भारत स्थित कार्यालय में हिन्दी सेवा में प्रशिक्षण के लिए बहाल की गई मीना कोटवाल को काम से बाहर निकालने का एक फैसला सुनाई दिया है। आखिर आपने मीना का चयन क्यों किया था? क्या महज यह प्रचारित करने के लिए किया था कि बीबीसी में भी दलित हैं।
मुझे पत्रकारिता के हजारों प्रशिक्षणर्थियों के साथ काम करने का मौका मिला है। राजस्थान जैसे सामंती प्रदेश के जिस श्रमिक परिवार की चार बहनों व भाईयों ने आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई नहीं की हो और उस परिवार की सबसे छोटी लड़की मीना ने तरह-तरह की मजदूरी करके अपने बल पर देश के सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थानों जैसे जामिया मीलिया इस्लामिया और भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) से पत्रकारिता का कोर्स किया तो उसके भीतर की इस ताकत को पहचाना जा सकता है। उसकी योग्यताओं को परखा जा सकता है। लेकिन उस अकेली दलित महिला को बीबीसी में सैकड़ों लोग बीबीसी के लायक प्रशिक्षित नहीं कर सकें। आप खुद सोचें कि इसका विश्लेषण कैसे किया जाना चाहिए। क्या यह अयोग्यता प्रशिक्षण देने वालों की नहीं है?
मैं मीना की बीबीसी-डायरी सुन रहा था। वह अम्बेडकर नगर में जाति को महसूस नहीं कर सकी क्योंकि वहां उसके ही जैसे लोग रहते हैं। लेकिन बीबीसी में उसका यह अपराध हुआ कि उसने महसूस करना शुरू कर दिया। ऐसे सैकड़ों लोगों का हमें अनुभव है कि दलित अपनी बस्ती से जब बाहर निकलता है तभी उसे जाति का एहसास होता है। जो वर्ण व्यवस्था की ऊपरी जाति के परिवार में पैदा होता है उसके स्वभाव में यह बुरी तरह से घुला मिला होता है कि वह समाज में ऊपर वाला सदस्य है। बीबीसी में मीना को यह बताया गया कि इंटरनेट के जमाने में कोई दलित नहीं होता। यह किस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाने की उद्घोषणा है? बीबीसी में काम करने वाले एक दूसरे जातिवादी ने घर लौटते हुए ड्राइवर से कहा कि अब आपके लोग भी हमारे साथ बैठेंगे। यह मीना की तरफ इशारा था। ये बीबीसी के दो लोग नहीं है। ये एक ही है क्योंकि जाति की तरह सोचते हैं। जाति कैसे एक समूह के रुप में वहां काम करती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बीबीसी रोजाना भारत में दलित होने की सजा भुगत रहे लोगों की कहानियों से रूबरू होता है। दलित बीबीसी की सामग्री भर नहीं है।
मीना ने जिन कठिन परिस्थितियों में अपना विकास किया है, उसमें उसकी ताकत की पहचान की जा सकती है। बीबीसी में उसने पाया कि वहां उन लोगों का वर्चस्व है जो कि एक दलित और वह भी स्त्री के भरोसे की ताकत को तोड़ने के लिए सदियों से प्रशिक्षित किए गए हैं। हिन्दू मिथक ग्रंथ महाभारत के दोर्णाचार्य द्वारा एकलव्य से अंगूठा मांगने का नया रूप है- आत्म विश्वास को तोड़ना। प्रशिक्षण लेने गई एक लड़की को डिप्रेशन का शिकार होना पड़े, उसे आत्महत्या के बारे में सोचना पड़े और तो और वह इतनी डरी हो कि अपने दफ्तर के करीब पहुंचकर यह सोचे कि उसका एक्सीटेंड हो जाए और उसे अपने दप्तर कई दिनों तक नहीं जाना पड़े, तो इस हालात का विश्लेषण किया जा सकता है। उसकी अपनी ताकत की पूंजी से बेदखल करने के जातीय वायरस के हमले के अलावा इसे किस रूप में देखा जा सकता है? एक उस व्यक्ति को डांट पड़ती हो, जो बशर्म हो चुका हो और चापलूसी की संस्कृति में ढला हो तो उसे डांट का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उस व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर डांट पड़े जो कि डांट को डांट की तरह ग्रहण करता हो, तो उसके लिए खाना पीना और सोना मुश्किल हो जाता है और वर्चस्ववादी संस्कृति में इसका हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। डांटने में अपमान और अपनत्व का फर्क आप जानते होंगे। भारतीय समाज में एक दलित व स्त्री को उसकी चेतना और अपेक्षाओं के साथ स्वीकार करने की संवेदना हर क्षण एक चुनौती की तरह खड़ी रहती है। मीना जो महसूस करती रही है उसे देखने वाले भी बीबीसी में हो सकते हैं। लेकिन वह सदियों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए नाकाफी है। उन्हें अपवाद के रूप में ही हम देख सकते हैं।
मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भारत में बीबीसी को जाति संस्था के रूप में बनने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करें। आप समाज शास्त्रियों का सहयोग लें और वास्तव में भारतीय समाज का आईना बनने की कोशिश करें। बहुत ही होनहार लोग उनके बीच हैं जो कि पिछड़े, दलित, आदिवासी कहे जाते हैं।
आशा है आपको मेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा होगा। यदि गलती से आपकी किसी भावना को चोट पंहुची हो, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप मीना के पूरे मामले को आईने पर पड़ी धूल को साफ करने के एक मौके के रुप में देखेंगे, यह विश्वास करता हूं।
आदर सहित
अनिल चमड़िया