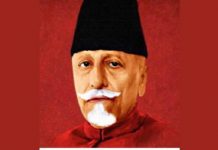हेमंत कुमार झा:पाकिस्तान से निबटने के लिये तो सेना है, रक्षा और विदेश विभाग का थिंक टैंक है, लेकिन मीडिया के उस वर्ग से कौन निबटेगा जो मूलतः जनविरोधी और शान्तिद्रोही बन चुका है? इसने पत्रकारिता की मौलिक अवधारणा की हत्या तो कब की कर दी थी और अब स्वयं देश के लिये एक बड़ा खतरा बन गया है।
विश्वसनीयता…जो मीडिया की आत्मा है, वह इसका साथ छोड़ चुकी है और उसकी प्राणहीन देह अब दुर्गंध के सिवा कुछ नहीं फैला रही।
नौबत यह है कि भारत-पाक के बीच उभरे तनावों और सैनिक कार्रवाइयों की सही जानकारी के लिये समझदार लोगों के पास अंतरराष्ट्रीय मीडिया के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया है। कुछेक भारतीय चैनल हैं जो संतुलित और वस्तुनिष्ठ खबरें देने की कोशिशें कर रहे हैं लेकिन विश्वसनीयता का संकट, जिसके कोहरे में भारतीय मीडिया घिर चुका है, इन संतुलित खबरों की सच्चाई के प्रति भी आस्था नहीं जगा पा रहा।
अधिकांश चैनल और उनके आत्ममुग्ध एंकर देशभक्ति को सत्ताधारी दल की दलाली में बदल चुके हैं। एंकरों की भाषा, उनका ‘बॉडी लैंग्वेज’ उनके परोक्ष राजनीतिक उद्देश्यों की खुलेआम चुगली करता है और…इसमें क्या आश्चर्य कि उन्हें इसकी कोई शर्म भी नहीं।
जिस तरह किसी नाटक-नौटंकी में उटपटांग हरकतें करते और अशालीन भाषा में बातें करते घटिया दर्जे के विदूषकों से किसी भी तरह के शर्म की अपेक्षा करना बेकार है, उसी तरह ये चैनल और उनके एंकर हैं।
मीडिया में राष्ट्रवाद की इतनी फूहड़ और भ्रामक प्रस्तुति ने राष्ट्र, सेना, सरकार, सत्ताधारी दल और सत्तासीन राजनेता के बीच के फर्क को पाट कर उन्हें एक ही धरातल पर ला दिया है।
पत्रकारिता के अध्येताओं के लिये भविष्य में यह एक रोचक अध्याय होगा कि किस तरह कुछेक हाथों में भारतीय चैनलों का मालिकाना हक सिमटता गया और पत्रकारों की जगह बोलती कठपुतलियों के माध्यम से अपने राजनीतिक और आर्थिक हित साधने की कवायदें चलती रहीं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उभार ने नई उम्मीदें जगाई थीं और लगा था कि दृश्य-श्रव्य का यह माध्यम सच को कुछ अधिक करीब से, कुछ अधिक बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकेगा। लेकिन, इसने पहली हत्या सच की ही की।
हालांकि, सच पर पहला आक्रमण प्रिंट मीडिया के दौर में ही हो चुका था। एक वक्त था जब छपे हुए शब्दों की विश्वसनीयता थी। धीरे-धीरे यह खंडित होती गई क्योंकि लोकतंत्र का हरण करने वाली शक्तियों को मीडिया के प्रभावों का अंदाजा था। उन्होंने अखबारों को शिकंजे में लेना शुरू किया।
किन्तु, प्रिंट मीडिया को पूरी तरह शिकंजे में लेना कभी संभव नहीं हो सका। कुछेक स्वतंत्र चेता संपादकों और निर्भीक रिपोर्टरों ने सच्चाई से मुठभेड़ कर जन सापेक्षता के नए प्रतिमान स्थापित किये।
अखबारों की साख पर धब्बे तो लगते रहे, संपादक के पदों पर बौद्धिक रूप से बौने या मालिक के राजनीतिक हितों के प्रति हितैषी लोगों को बिठाया जाने लगा, लेकिन तब भी, न्यूनतम विश्वसनीयता बनी रही।
1990 के दशक में संपादकों के पदों का ही अवमूल्यन कर दिया गया। इसने प्रिंट मीडिया की साख को निर्णायक धक्का पहुंचाया। अब अधिकतर मालिकान ही संपादकों का दायित्व निभाने लगे। जाहिर है, सच से अखबारों का नाता टूटने लगा।
1990 के दशक में ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास और विस्तार के साथ निजी समाचार चैनलों का भी आगमन हुआ। उसके बाद तो तमाम प्रतिमानों के ध्वस्त होने का दौर शुरू हो गया।
पहले खबरों और मनोरंजन का फर्क मिटा, फिर सनसनी फैलाने के लिये खबरों के साथ खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति पनपी…और तब…खबरों की जगह दलाली और प्रस्तोताओं की जगह दलालों ने लेनी शुरू की। नए-नए मीडिया घराने अस्तित्व में आए जिन्हें पत्रकारिता से कोई लेना-देना नहीं था। जाहिर है, उन्होंने ऐसे लोगों की भर्त्ती की जो उनके राजनीतिक, प्रकारान्तर से व्यावसायिक उद्देश्यों के वाहक बने।
आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना जनविरोधी बन चुका है कि उन्हें देखना, उनके साथ थोड़ा भी वक्त बिताना अपना दिमाग प्रदूषित करना है। वे प्रदूषण फैलाने के सिवाय और कुछ नहीं कर रहे। वे कुछ और कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी नियुक्ति ही इसीलिये की गई है।
आतंकवादियों से निबटने के लिये देश में सक्षम तंत्र है और वे उनसे निबट भी रहे हैं। लेकिन…इन चैनलों से, इनके दलाल एंकरों से, जिन्होंने आम जन के जरूरी मुद्दों को पत्रकारिता के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया है, निबटने के लिये रास्तों की तलाश करनी होगी।
(हेमंत कुमार झा)